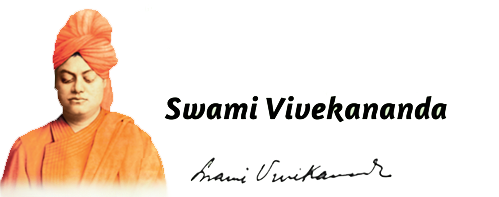२. आश्चर्य की बात है कि सभी धर्म एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मनुष्य पहले निष्पाप और पवित्र था, पर आज उसकी अवनति हो गयी है, इस भाव को फिर वे रूपक की भाषा में, या दर्शन की स्पष्ट भाषा में अथवा कविता की सुन्दर भाषा में क्यों न प्रकाशित करें, पर वे सब के सब अवश्य इस एक तत्त्व की घोषणा करते हैं। (२/५)
३. अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप एक ही है, वह अनन्त और सर्वव्यापी है, और यह प्रातिभासिक जीव मनुष्य के इस वास्तविक स्वरूप का एक सीमाबद्ध भाव मात्र है। इसी अर्थ में पूर्वोक्त पौराणिक तत्व भी सत्य हो सकते हैं कि प्रातिभासिक जीव, चाहे वह कितना ही महान् क्यों न हो, मनुष्य के इस अतीन्द्रिय, प्रकृत स्वरूप का धुँधला प्रतिबिम्ब मात्र है। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप – आत्मा – कार्य-कारण से अतीत होने के कारण, देश-काल से अतीत होने के कारण, अवश्य मुक्तस्वभाव है। वह कभी बद्ध नहीं थी, न ही बद्ध हो सकती थी। यह प्रातिभासिक जीव, यह प्रतिबिम्ब, देश-काल-निमित्त के द्वारा सीमाबद्ध होने के कारण बद्ध है। अथवा हमारे कुछ दार्शनिकों की भाषा में, ‘प्रतीत होता है, मानो वह बद्ध हो गयी है, पर वास्तव में वह बद्ध नहीं है।’ (२/१०-११)
४. सम्पूर्ण शास्त्र एवं विज्ञान मनुष्य के रूप में प्रकट होनेवाली इस आत्मा की महिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह समस्त ईश्वरों में श्रेष्ठ है, एकमात्र वही ईश्वर है, जिसकी सत्ता सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी। (२/२१२)
५. आदमी भ्रमवश अपने से बाहर विभिन्न देवताओं की तलाश में रहता है, पर जब उसके अज्ञान का चक्कर समाप्त होता है, तो वह पुनः लौटकर अपनी आत्मा पर आ टिकता है। जिस ईश्वर की खोज में वह दर दर भटकता रहा, वन-प्रान्तर तथा मन्दिर-मस्जिद को छानता रहा, जिसे वह स्वर्ग मैं बैठकर संसार पर शासन करनेवाला मानता रहा, वह कोई अन्य नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही आत्मा है। वह मैं है, और मैं वह। मैं ही (जो आत्मा हूँ) ब्रह्म हूँ, मेरे इस तुच्छ ‘मैं’ का कभी अस्तित्व नहीं रहा। (२/२१३)
६. ईश्वरोपासना करने के लिए प्रतिमा आवश्यक है, तो उससे कहीं श्रेष्ठ मानव-प्रतिमा मौजूद ही है। यदि ईश्वरोपासना के लिए मन्दिर निर्माण करना चाहते हो, तो करो, किन्तु सोच लो कि उससे भी उच्चतर, उससे भी महान् मानव देह रूपी मन्दिर तो पहले से ही मौजूद है। (८/२३)
७. जीवित ईश्वर तुम लोगों के भीतर रहते हैं, तब भी तुम मन्दिर, गिरजाघर आदि बनाते हो और सब प्रकार की काल्पनिक झूठी चीजों में विश्वास करते हो। मनुष्य-देह में स्थित मानव-आत्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। पशु भी भगवान् के मन्दिर हैं, किन्तु मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ मन्दिर है – ताजमहल जैसा। यदि मैं उसकी उपासना नहीं कर सका, तो अन्य किसी भी मन्दिर से कुछ भी उपकार नहीं होगा। जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य-देहरूपी मन्दिर में उपविष्ट ईश्वर की उपलब्धि कर सकूँगा, जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख भक्तिभाव से खड़ा हो सकूँगा और वास्तव में उनमें ईश्वर देख सकूँगा, जिस क्षण मेरे अन्दर यह भाव आ जायगा, उसी क्षण मैं सम्पूर्ण बन्धनों से मुक्त हो जाऊँगा – बाँधनेवाले पदार्थ हट जायँगे और मैं मुक्त हो जाऊँगा। (८/२९-३०)
८. यह आदर्श अवस्था वह है, जिसमें मनुष्य का अहंभाव पूर्णतया नष्ट हो जाता है, उसका स्वत्व-भाव लुप्त हो जाता है, जब उसके लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसे वह ‘मैं’ और ‘मेरी’ कह सके, जब वह पूर्णतया आत्म-विसर्जन कर देता है, मानो अपनी आहुति दे देता है। इस प्रकार अवस्थापन्न व्यक्ति के अन्तर में स्वयं ईश्वर निवास करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की अहं-वासना पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी है, एकदम निर्मूल हो गयी है। यह है आदर्श व्यक्ति। (७/२२७)
९. जिस परिमाण में मनुष्य इन्द्रियपरायणता को छोड़कर उच्च भावजगत् में अवस्थान करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, जिस परिमाण में वह विशुद्ध चिन्तन रूपी प्राणवायु फेफड़ों के भीतर खींचने में समर्थ हो जाता है तथा जितने अधिक समय तक वह उस उच्च अवस्था में रह सकता है, केवल इसी आधार पर उसका विकास आँका जा सकता है। (९/२५९)
१०. पहले हमें ईश्वर बन लेने दो। तत्पश्चात् दूसरों को ईश्वर बनाने में सहायता देंगे। बनो और बनाओ, यही हमारा मूल-मंत्र रहे।
ऐसा न कहो कि मनुष्य पापी है। उसे यह बताओ कि तू ब्रह्म है। यदि कोई शैतान हो, तो भी हमारा कर्तव्य यही है कि हम ब्रह्म का ही स्मरण करें, शैतान का नहीं। (९/३७९-८०)
११. जब तुम अपने आपको शरीर समझते हो, तुम विश्व से अलग हो; जब तुम अपने आपको जीव समझते हो, तब तुम अनन्त अग्नि के एक स्फुलिंग हो; जब तुम अपने आपको आत्मस्वरूप मानते हो, तभी तुम विश्व हो। (१०/२१३)
१२. चालाकी से कोई बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता। प्रेम, सत्यानुराग और महान् वीर्य की सहायता से सभी कार्य सम्पन्न होते हैं। तत् कुरु पौरुषम, इसलिए पुरुषार्थ को प्रकट करो। (४/३१७)
१३. हम नियम नहीं चाहते, हम चाहते हैं नियम को तोड़ने का सामर्थ्य। हम नियमों से बाहर चले जाना चाहते हैं। यदि तुम नियमों से बँधे हो, तो मिट्टी के ढेले की भाँति निर्जीव हो। प्रश्न यह नहीं है कि तुम नियमातीत हो या नहीं; किन्तु यह धारणा कि हम नियमातीत हैं, समस्त मानव इतिहास की आधारशिला है। (९/१६७)
१४. प्रत्येक मनुष्य पहले से ही अनन्त है, केवल इन सब विभिन्न अवस्था-चक्ररूपी द्वारों या प्रतिबन्धों ने उसे बद्ध कर रखा है। इन प्रतिबन्धों को हटाने मात्र से ही उसकी वह अनन्त शक्ति बड़े वेग के साथ अभिव्यक्त होने लगती है। (१०/३८२)
१५. योगी कहते हैं कि योगी के अतिरिक्त अन्य सब मानो गुलाम हैं – खाने-पीने के गुलाम, अपनी स्त्री के गुलाम, अपने लड़के-बच्चों के गुलाम, रुपये-पैसे के गुलाम, स्वदेशवासियों के गुलाम, नाम-यश के गुलाम, जलवायु के गुलाम, इस संसार के हज़ारों विषयों के गुलाम! जो मनुष्य इन बन्धनों में से किसी में भी नहीं फँसें, वे ही यथार्थ मनुष्य हैं – यथार्थ योगी हैं। (१०/३९०-९१)
१६. प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके अपने वर्तमान उन्नति-क्षेत्र के भीतर स्वयं को उन्नत बनाने के लिए अवसर विद्यमान है। हम अपना नाश नहीं कर सकते, हम अपने भीतर की जीवनी शक्ति को नष्ट या दुर्बल नहीं कर सकते, परन्तु उस शक्ति को विभिन्न दिशा में परिचालित करने के लिए हम स्वतन्त्र हैं। (१०/३७६)
१७. व्यावहारिक और शरीर से सबल होने की शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे केवल बारह नर-केसरी संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं; परन्तु लाख-लाख भेड़ों द्वारा यह नहीं होने का। और दूसरे, किसी व्यक्तिगत आदर्श के अनुकरण की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, चाहे वह आदर्श कितना ही बड़ा क्यों न हो। (१०/३७२)
१८. मनुष्य एक छोटे बक्से में कुण्डलित अनंत स्प्रिंग (infinite spring) जैसा है, जो कि अपने को खोलने का प्रयत्न कर रहा है। हम लोग जो भी सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, वह इस अभिव्यक्ति का प्रयत्न मात्र है। (९/११८)
१९. आप तो ईश्वर की सन्तान हैं, अमर आनंद के भागी हैं, पवित्र और पूर्ण आत्मा हैं। आप इस मर्त्यभूमि पर देवता हैं। आप भला पापी? मनुष्य को पापी कहना ही पाप है, वह मानवस्वरूप पर घोर लांछन है। आप उठें! हे सिंहो! आयें, और इस मिथ्या भ्रम को झटककर दूर फेंक दें कि आप भेंड़ हैं। (१/१२)
२०. हम सभी एक जीवाणु-कोष से उत्पन्न हुए हैं और हम लोगों में जो कुछ भी शक्ति है, वह उसीमें कुण्डलीरूप में बैठी थी। तुम लोग यह नहीं कह सकते कि वह खाद्य में से आयी है; ढेर की ढेर खाद्य-सामग्री लेकर एक पर्वत बना डालो, किन्तु देखोगे उसमें से कोई शक्ति नहीं निकलती। हम लोगों के भीतर शक्ति पहले से ही अव्यक्त भाव में निहित थी, और वह थी अवश्य। इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा के भीतर अनन्त शक्ति भरी पड़ी है, मनुष्य को उसका ज्ञान हो या न हो। उसे केवल जानने की ही अपेक्षा है। धीरे धीरे मानो वह अनन्त शक्तिमान दैत्य जाग्रत होकर अपनी शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर रहा है और जैसे जैसे वह सचेतन होता जाता है, वैसे वैसे एक के बाद एक उसके बन्धन टूटते जाते हैं, शृंखलाएँ छिन्नभिन्न होती जाती हैं; और वह दिन अवश्य ही आयगा, जब वह अपनी अनंत शक्ति के पूर्ण ज्ञान के साथ अपने पैरों पर उठ खड़ा होगा। आओ, हम सब लोग उस महिमामयी निष्पत्ति को शीघ्र लाने में सहायता करें। (८/४७)